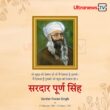सियारामशरण गुप्त हिन्दी के साहित्यकार थे। वे प्रसिद्ध हिन्दी कवि मैथिलीशरण गुप्त के अनुज थे। सियारामशरण गुप्त का जन्म सेठ रामचरण कनकने के परिवार में चिरगाँव, झांसी में हुआ था।
सियारामशरण गुप्त जीवनी -Siyaramsharan Gupt Biography
| जन्म | 4 सितंबर, 1895 |
| भाई | मैथिलीशरण गुप्त |
| उल्लेखनीय कार्य | मौर्य विजय(1914), अनाथ(1917) |
| मृत्यु | 29 मार्च 1936 |
जीवन – Life
प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने घर में ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा सीखी। सन् 1929 ई. में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा गाँधी के सम्पर्क में आये। कुछ समय वर्धा आश्रम में भी रहे। सन् 1940 में चिरगांव में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का स्वागत किया। वे सन्त विनोबा भावे के सम्पर्क में भी आये। उनकी पत्नी तथा पुत्रों का निधन असमय ही हो गया था अतः वे दु:ख वेदना और करुणा के कवि बन गये। 1914 में उन्होंने अपनी पहली रचना मौर्य विजय लिखी। सन् 1910 में इनकी प्रथम कविता ‘इन्दु’ प्रकाशित हुई।
काव्य रूपों की दृष्टि से उन्मुक्त नृत्य नाट्य के अतिरिक्त उन्होंने पुण्य पर्व नाटक (1932), झूठा सच निबंध संग्रह (1937), गोद, आकांक्षा और नारी उपन्यास तथा लघुकथाओं (मानुषी) की भी रचना की थी। उनके गद्य साहित्य में भी उनका मानव प्रेम ही व्यक्त हुआ है। कथा साहित्य की शिल्प विधि में नवीनता न होने पर भी नारी और दलित वर्ग के प्रति उनका दयाभाव देखते ही बनता है। समाज की समस्त असंगतियों के प्रति इस वैष्णव कवि ने कहीं समझौता नहीं किया किंतु उनका समाधान सर्वत्र गांधी जी की तरह उन्होंने वर्ग संघर्ष के आधार पर न करके हृदय परिवर्तन द्वारा ही किया है, अत: “गोद’ में शोभाराम मिथ्या कलंक की चिंता न कर उपेक्षित किशोरी को अपना लेता है; “अंतिम आकांक्षा’ में रामलाल अपने मालिक के लिए सर्वस्व त्याग करता है और “नारी’ के जमुना अकेले ही विपत्तिपथ पर अडिग भाव से चलती रहती है। गुप्त जी की मानुषी, कष्ट का प्रतिदान, चुक्खू प्रेत का पलायन, रामलीला आदि कथाओं में पीड़ित के प्रति संवेदना जगाने का प्रयत्न ही अधिक मिलता है। जाति वर्ण, दल वर्ग से परे शुद्ध मानवतावाद ही उनका कथ्य है। वस्तुत: अनेक काव्य भी पद्यबद्ध कथाएँ ही हैं और गद्य और पद्य में एक ही उक्त मंतव्य व्यक्त हुआ है। गुप्त जी के पद्य में नाटकीयता तथा कौशल का अभाव होने पर भी संतों जैसी निश्छलता और संकुलता का अप्रयोग उनके साहित्य को आधुनिक साहित्य के तुमुल कोलाहल में शांत, स्थिर, सात्विक घृतपीद का गौरव देता है जो हृदय की पशुता के अंधकार को दूर करने के लिए अपनी ज्योति में आत्म मग्न एवं निष्कंप भाव से स्थित है।
प्रमुख रचनाएँ
- खण्ड काव्य– मौर्य विजय(1914), अनाथ(1917), आर्द्रा(1927), विषाद(1925), दूर्वा दल(1924), आत्मोत्सर्ग(1931), पाथेय(1933), मृण्मयी(1936), बापू(1937), उन्मुक्त(1940), दैनिकी(1942), नकुल(1946), सुनन्दा और गोपिका।
- कहानी संग्रह– मानुषी
- नाटक– पुण्य पर्व
- अनुवाद– गीता सम्वाद
- नाट्य– उन्मुक्त गीत
- कविता संग्रह– अनुरुपा तथा अमृत पुत्र
- काव्यग्रन्थ– दैनिकी नकुल, नोआखली में, जय हिन्द, पाथेय, मृण्मयी तथा आत्मोसर्ग।
- उपन्यास– अन्तिम आकांक्षा तथा नारी और गोद।
- निबन्ध संग्रह– झूठ-सच।
- पद्यानुवाद– ईषोपनिषद, धम्मपद और भगवत गीता
सम्मान
उन्हें दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन्1962 में ‘सरस्वती हीरक जयन्ती’ के अवसर पर सम्मानित किया गया। 1941 में उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा “सुधाकर पदक’ प्रदान किया गया। उनकी समस्त रचनाएं पांच खण्डों में संकलित कर प्रकाशित हैं।
लम्बी बीमारी के बाद 29 मार्च 1936 ई. को उनका निधन हो गया।