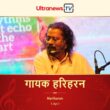यूँ तो भारत के हर राज्य की बुनावट ऐसी है कि उसके हर एक रेशे से अलग इतिहास अपनी बुढ़ापे की लाठी लिए बैठ नज़र आता है और उसी रेशे से हर रोज एक नयी कहानी की किलकारी गूंज उठती है।
तमाम किस्से-कहानियों को समेटते हुए इस लेख को जन्म दिया जा रहा है, जिसमें हम लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है(आजकल बागों का शहर), की सर-जमीं से रु-ब-रु हो सकेंगे।
इस शहर या भारत के किसी भी शहर की बसावट का सही सही अनुमान लगाने जाएं तो कई किताबें ग्रंथ को खंगाल कर भी शायद जानकारी अप्रायप्त ही रहे, फिर भी जितनी जानकारी हमारे पास है और इंटरनेट के द्वारा इस लेख के को लखनऊ के लोगों और उस शहर के बारे में ईछुक लोगों के लिए रोचकजांकरिपूर्ण बनेंगे।
लखनऊ : इतिहास

लखनऊ की उत्पत्ति की प्राचीनता सूर्यवंशी राजवंश के युग से जुड़ी हुई है, यह शहर कोसल के प्राचीन महाजनपद का अभिन्न अंग था। जिस पर सूर्यवंशी (इक्ष्वाकु) राजवंश का शासन था, जिसकी राजधानी अयोध्या एवं तत्पश्चात श्रावस्ती थी। परम्परानुसार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के कर्तव्यनिष्ठ और स्नेही भाई लक्ष्मण के सम्मान में इस शहर का नाम लखनपुरी रखा गया था और फिर अंततः इस शहर का नाम लखनऊ पड़ा, इस बात को विश्वसनीय बनाने के लिए शहर के शहर के उत्तर-पश्चिम में स्थित लक्ष्मण टीला है। हालाँकि, निश्चित अभिलेखों के अभाव के कारण जिले के वर्तमान स्वरूप में इसके गठन की सटीक तिथि अनिश्चित बनी हुई है।
इतिहास के वर्ष 1350 से प्रारंभ होता है इस शहर में अलग-अलग शाही संस्थानों का आधिपत्य। जो क्रमशः है, दिल्ली सल्तनत, शर्की सल्तनत, राजसी मुगल साम्राज्य, अवध के स्वदेशी नवाब, उद्यमी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंततः ब्रिटिश राज, जिनमें से प्रत्येक ने इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। मुग़लकाल के सम्राट जलाल-उद-दीन मोहम्मद अकबर की आइन-ए-अकबरी के एक विवरण से मालूम होता है की इस शहर का महत्व 1580ई से प्रारंभ हुआ, जब मुगल सम्राट अकबर ने अवध के प्रशासनिक प्रांत की स्थापना की। 1722 में शौकत जंग (1680-1739) की नवाब वजीर के रूप में नियुक्ति ने नवाबों के वंश की स्थापनाको चिह्नित किया।

अवध की राजधानी शुरू में फैजाबाद में स्थित थी, हालाँकि, तत्पश्चात नवाब आसफ-उद-दौला ने 1775 में राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित करने का फैसला किया, जिससे शहर को राजधानी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। नादिर शाह द्वारा दिल्ली की लूटपाट, सिखों, मराठों और रोहिल्लाओं के आक्रमण और 1803 में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा दिल्ली पर कब्जे के कारण मुगल सत्ता का पतन हुआ, जिसके कारण प्रांतीय गवर्नरों का उदय हुआ एवं अवध सूबे की सहवर्ती स्वतंत्रता में वृद्धि हुई।
इस स्थिति के परिणामस्वरूप, मुगल दरबार से कलाकारों और सांस्कृतिक दिग्गजों का प्रवास आसान हो गया, जिन्हें अवध के बढ़ते दरबार में संरक्षण मिला, जिससे दरबारी शिष्टाचार और परिष्कार की विशेषता वाली एक अनूठी सांस्कृतिक लोकाचार की उन्नति हुई।
यूरोपीयकरण की प्रक्रिया आसफ-उद-दौला के शासनकाल के दौरान प्रारम्भ हुई, जैसा कि ब्रिटिश रेजिडेंट जॉन ब्रिस्टो से यूरोपीय शैली में एक घर डिजाइन करने के उनके अनुरोध से स्पष्ट होता है।
गाज़ी-उद-दीन हैदर के शासनकाल में अवध के वास्तुशिल्पीय दृश्य में महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसमें छोटा छतर मंजिल, मोती महल परिसर के कुछ भाग और शाह नजफ इमामबाड़ा जैसे स्मारकों का निर्माण किया गया। इसके अलावा, नासिरुद्दीन हैदर द्वारा छतर मंजिल परिसर की पूर्णता कर एवं कोठी दर्शन बिलास का निर्माण कर इस प्रवृत्ति को और मजबूत बनाया। वाजिद अली शाह के निर्माण , जिनमें सिकंदरबाग महल, कैसरबाग महल परिसर और उनके पिता अमजद अली शाह का मकबरा शामिल है, इस संकरित शैली के चरमोत्कर्ष को प्रदर्शित करते हैं।
प्राचीन काल से लेकर नवाबों के शासनकाल तक, लखनऊ ने एक गहरा परिवर्तन देखा है, जो मुगल और इंडो-यूरोपीय वास्तुकला के संयोजन से एक जीवंत, वैश्विक शहर में विकसित हुआ है। अवध की एक समय में शांत राजधानी अब एक समृद्ध महानगर में खिल गई है, जो आधुनिकता को अपनाते हुए अपने ऐतिहासिक अतीत की सार को संरक्षित करती है।

वर्तमान परिदृश्य में आधुनिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विस्तृत सचिवालय, विधान सभा और अनेकों सरकारी संस्थान हैं। शहर की दृश्यावली शॉपिंग मॉल, उच्च श्रेणी के आवासीय परिसरों और कुशल मेट्रो रेल प्रणाली के आगमन से परिवर्तित हुई है, जिसने संपर्क को सुव्यवस्थित और विकास को सुगम बनाया है।
लखनऊ : संस्कृति (Lucknow – Culture)
‘लखनऊ तहजीब’ के नाम से प्रसिद्ध यह शानदार सांस्कृतिक समृद्धि सदियों से एक साथ रहने वाले दो समुदायों की संस्कृतियों को जोड़ती है, समान रुचियों को साझा करती है, एक आम भाषा – उर्दू बोलती है। लखनऊ की कई सांस्कृतिक विशेषताएँ और रीति-रिवाज आज जीवित किंवदंतियाँ बन गए हैं। इसका श्रेय अवध के नवाबों को जाता है, जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी ली और लोगों को पूर्णता की एक दुर्लभ डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।
‘लखनऊ’, यह नाम ‘लखौरी’ ईंटों की वास्तुकला की खूबसूरती, ‘इत्र’ की खुशबू, संगीत के सुर, नर्तकियों की खनक, ‘दशहरी’ आम, ‘मलाई’ और ‘गुलाब रेवड़ियों’ की मिठास और निश्चित रूप से ‘मेहमान नवाजी’ का पर्याय है।

अपनी बोली, मनोरंजन, पहनावे और शिष्टाचार में नफासत के लिए मशहूर लखनऊ को ‘आदब का शहर’ भी कहा जाता है। दरअसल, यहीं पर मेहमाननवाज़ी का सही अर्थों में अनुभव किया जा सकता है। इस अनोखे शहर की समृद्धि में विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का योगदान है।
इस शहर की बात करते हुए, उर्दू भाषा का ज़िक्र करना ज़रूरी है। ग़ज़लें, शायरी, भावपूर्ण नृत्य रूप, रंग-बिरंगे त्यौहार, चहल-पहल वाले चौक और पतंगबाज़ी, बटेरबाज़ी और कबूतरबाज़ी जैसे कई रोमांचक खेल यहाँ की पहचान है।
शाही संरक्षण में कथक, ठुमरी, ख्याल, दादरा, गजल, कव्वाली और शेर-ओ-शायरी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गए। इस्लामी शिक्षा के केंद्र के रूप में लखनऊ ने अनीस, दबीर, इमाम-बक्श ‘नासिका’, मिर्ज़ा मोहम्मद जैसे प्रसिद्ध कवियों के अधीन लखनऊ कविता स्कूल के गठन को देखा। रजा खान बर्क, आतिश, मिर्ज़ा शौक असर, जोश और अन्य। गजलों के अलावा, लंबी कथात्मक कविता का एक और रूप जिसके लिए लखनऊ प्रसिद्ध है, वह है।
मसनव । उर्दू में शोकगीत लेखन भी तीन रूपों- ‘ मर्सिया ‘, ‘सलाम’ और ‘नौहा ‘ के माध्यम से एक नई ऊंचाई पर पहुंचा । एक भाषा के रूप में उर्दू ने लखनऊ में पूर्णता की एक दुर्लभ डिग्री प्राप्त की।

‘चौक’ शब्द लखनऊ का पर्याय बन गया है। ‘चौक’ ने लखनवी संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह वह केंद्र बिंदु है जिसके इर्द-गिर्द व्यापारी, उत्कीर्णक, चित्रकार, कारीगर, बुनकर, गायिकाएँ और नाचने-गाने वाली लड़कियाँ पनपीं और बढ़ीं। बीते सालों का यह मुख्य बाज़ार ज़्यादा नहीं बदला है। लेकिन बदलाव ज़रूर हुआ है। इसकी गुनगुनाहट और जीवंत विशेषताएँ आधुनिक समय के संदर्भ में लखनवी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं।
लखनऊ – वास्तुकला (Architect)
लोग ऐसी जगहें बनाते हैं जो शहर में बदल जाती हैं और जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करती हैं और इसकी संस्कृति, परंपराओं, दृष्टिकोणों और प्रतीकात्मक ऐतिहासिक प्रभावों के माध्यम से बदलावों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र मुगल सम्राटों (नवाबों) के सार और इमारतों और इसकी नगर नियोजन के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को देखने के लिए एक उल्लेखनीय स्थल है।
लखनऊ की वास्तुकला अपने शाही इमामबाड़ों, महलों, उद्यानों और आवासीय भवनों के लिए जानी जाती है। सदी की शुरुआत में लखनऊ के नवाबों की खासियत इमारतों में बारोक शैली को फिर से तैयार करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था।
अवध और नवाबी शैली
मुगल बादशाहों के आक्रमण ने अवध को 18वीं सदी की शुरुआत में अस्तित्व में ला दिया, जो खुद को शहर का नवाब कहते थे, न कि राजा। पहले और दूसरे नवाब के शासन में, प्रशासन और क्षेत्र के विकास के बजाय व्यक्तिगत हितों को संतुष्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उन्होंने जो प्रभाव दिखाया, उसने उन्हें ब्रिटिश संपत्तियों के साथ युद्ध करने और कर और राजस्व वसूलने के लिए प्रेरित किया। जब तक अवध के चौथे नवाब आसफ़ुद्दौला ने अपनी राजधानी लखनऊ में स्थानांतरित नहीं कर दी, तब तक कला और संस्कृति की ओर संक्रमण और वास्तुकला से जुड़े शहर की उदारता ने लखनऊ को अन्य क्षेत्रों के आसपास एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया।

कई मकबरे की संरचनाओं को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है जो शाही प्रोसेसर के रूप में अपनी जीवंत पहचान के प्रति नवाबों के उत्साह को दर्शाती हैं। सत्तारूढ़ नवाब ने अपने लिए एक नया महल बनवाया और अंधविश्वासों के अनुसार पिछले वाले को त्याग दिया। सटीकता के साथ और अधिक आश्चर्यजनक स्मारक बनाने और इमामों के प्रति उनके उत्साह के उद्देश्य से, लखनऊ ने स्मारकों, औपनिवेशिक घरों, बाज़ारों, मकबरों, मस्जिदों, इमामबाड़ों, महलों और उद्यानों से सजे धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष स्मारकों की शानदार संरचना देखी है।
धार्मिक वास्तुकला
मकबरे, इमामबाड़े और मस्जिद जैसी स्मारकीय इमारतें वास्तुकला के पारंपरिक तत्वों को दर्शाती हैं,धार्मिक स्मारकों में इस्तेमाल किये गए वास्तुशिल्प कला के तत्व वर्षों से एक जैसी ही रही है, वास्तुकला की इस शैली में, इमारतों में गुंबदों के भीतर जटिल विवरण, गुंबदों के साथ ऊंची मीनारें, प्रवेश द्वार में सजावटी तत्व के रूप में मछली, एक उच्च प्लिंथ बेस, मठ, मेहराब, आर्केड और कियोस्क होते हैं।
रूमी दरवाज़ा

इस दरवाजे के बनाने के पीछे का उद्देश्य है आकाल के समय लोगों को रोजगार देना के लिए बनाया गया, उस समय इसके बनने से करीब 22,000 मजदूरों के घर अन्न पहुँच।
इस दारवाज़े की विशेषताएं-
- यह दरवाज़ा कांस्टेनटिनोपल के एक ऐतिहासिक दरवाज़े के मॉडल पर बना है
- यह दरवाज़ा करीब 60 फ़ुट ऊंचा है
- इसके ऊपरी हिस्से में एक आठ मुखी छतरी है
- इस दरवाज़े में इंडो-इस्लामिक शैली के साथ-साथ राजपूत शैली भी दिखती है
- यह दरवाज़ा बड़े और छोटे इमामबाड़े को जोड़ता है
- यह दरवाज़ा पुराने लखनऊ शहर के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है
- रूमी दरवाज़े की सजावट में हिंदू-मुस्लिम कला का सम्मिश्रण देखने को मिलता है
- रूमी दरवाज़े की बाहरी मेहराब को नागफ़नों से सजाया गया है

यह लखनऊ में अवधी वास्तुकला के उदाहरणों में से एक है, जिसे 1784 में नवाब आसफ उद दौला ने बनवाया था। रूमी दरवाज़े के वास्तुशिल्प विवरण इस तरह से हैं कि वे मुगलों के जीवन जीने के तरीके को दर्शाते हैं। उल्टे वी-धनुषाकार प्रवेश द्वार का प्रतिनिधित्व चिकनकारी कपड़ों की स्थानीय शैली को दर्शाता है। दरवाज़ा छोटा और बड़ा इमामबाड़ा के बीच एक कड़ी की तरह काम करता है, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल में तुर्की गेट से अपनी प्रेरणा ली। 60 फीट ऊंचे गेट में लाल पत्थर की संरचना थी जिसके बाद सजावटी मेहराबों के लिए ईंटों की परतों का इस्तेमाल किया गया था।
लखनऊ और खान-पान
कबाब और शर्मा की चाय

1722 ईस्वी में, इस शहर को अपना पहला नवाब, बुरहान-उल-मुल्क सआदत अली खान मिला, जो मूल रूप से निशापुर, (सफावी) फ़ारस का था। इसने, नवाबों की एक पूरी श्रृंखला द्वारा संरक्षित, शाही संस्कृति के साथ ही, उत्तम स्वाद और परिष्कार की भी नींव रखी। सआदत अली खान ने अवध क्षेत्र का विकास किया और फैजाबाद में अपनी पहली राजधानी स्थापित की। हालांकि ये नवाब असफ़-उद-दौला (1775-1797 ईस्वी) थे, जिन्होंने 1775 ईस्वी में लखनऊ को अवध की राजधानी बनाया।
लखनऊ के लोगों ने चाय को अपने दिल में एक विशेष स्थान दिया हुआ । चाय के एकदम गरमा-गरम कप और बन-मक्खन या समोसे के नाश्ते के लिए सबसे अच्छी जगह हज़रतगंज में स्थित शर्मा जी की चाय है। यहाँ के शानदार कबाब बेशक़ इस शहर के सबसे रोमांचक खाद्य पदार्थों में से एक हैं। टुंडे-के-कबाब उत्तर प्रदेश के बाहर के क्षेत्रों में भी अपनी “मुँह में घुल जाने वाली” और नरम चिकनी बनावट के लिए जाने जाते हैं। टुंडे कबाबी की दूकान को 1905 में चौक बाजार में हाजी मुराद अली द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने पतंग उड़ाते समय छत से गिरने के बाद अपना एक हाथ खो दिया था, जिससे उनका उक्त उपनाम पड़ा था। उनकी खासियत थी गलौटी-कबाब (गलावटी कबाब)।

यह दुकान जोकि अब 110 साल पुरानी हो गई है अभी भी उत्सुकता से इंतजार कर रहे स्थानीय लोगों को गलौटी-कबाब बेचती है। बहुत दिलचस्प बात यह है कि इन कबाबों के इतिहास की जड़ें 17वीं शताब्दी से जुड़ी हुई हैं। उम्र बढ़ने के साथ ही लखनऊ के तत्कालीन शाही नवाब, असफ़-उद-दौला ने अपने दांतों को खोना शुरू कर दिया था। हालांकि उनकी ज़ुबान को कबाब के स्वाद का चस्खा लग चुका था। इसलिए, उन्होंने घोषणा किया कि जो कोई भी एक ऐसा विशेष कबाब तैयार करेगा जिसे चबाने की आवश्यकता नहीं होगी उसे शाही संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कबाब की अन्य किस्मों में काकोरी-कबाब, शम्मी-कबाब, सीख-कबाब और कई स्थानीय विविधताएँ शामिल हैं।
बिरयानी
लखनवी भोजन के मुख्य भोज में शामिल है शाश्वत रूप से पसंद की जाने वाली बिरयानी। चौक बाजार की इदरीस की बिरयानी या वाहिद की बिरयानी में अवधी-बिरयानी अच्छे कारणों की वजह से स्थानीय बुनियादी भोज्य पदार्थ है

इसका देसी उत्कृष्ट स्वाद और मुँह में पानी ले आने वाली इसकी ज़बरदस्त सुगंध ही इसकी विशेषताएँ हैं, जो इसका विरोध करना मुश्किल बनाते हैं। कोलकाता-बिरयानी या हैदराबादी-बिरयानी के विपरीत, इसमें न तो अंडे पड़ते हैं और ना ही आलू और ना ही बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, बल्कि यह मांस के प्राकृतिक स्वाद पर केंद्रित होती है।
कुलचे-निहारी
लखनऊ का एक और अनोखा व्यंजन कुलचे-निहारी है जिसका सबसे अच्छा अनुभव चौक बाजार में स्थित रहीम्स के यहाँ मिलता है। ज़्यादातर लोग लखनवी भोजन यात्रा को इसके बिना अधूरा मानते हैं। मांस के नरम टुकड़ों को पारंपरिक भारतीय मसालों के साथ रगड़कर रात भर धीमी आँच पर पकाया जाता है।
खस्ता-कचौड़ी

एक और नवाबी स्वादिष्ट भोजन है खस्ता-कचौड़ी ,, जोकि लखनऊ के अमीनाबाद में रत्ती लाल की दुकान में मिलने वाला एक लोकप्रिय नाश्ता पकवान है। आटे की छोटी रोटी को घी में तलकर कचौड़ी तैयार की जाती है जिसको मसालेदार छोले सब्ज़ी के साथ, ऊपर से ताज़ा कटा प्याज़ और मिर्ची के दो टुकड़ों, या सूखे मसालेदार आलू डालकर, परोसा जाता है। इसकी भरपूर स्वादिष्टता और रुचिरता हर सुबह जल्दी उठने की एक अच्छी वजह प्रदान करती है!
शाही टुकड़ा और अन्य मीठे व्यंजन

सारे शहर के सार को एक टुकड़े में समेटने वाला शाही-टुकड़ा, एक प्रकार की मिठाई या ब्रेड पुडिंग होता है जिसे सिंकी हुई डबल रोटी, मावा (कंडेन्स्ड मिल्क), चीनी का शीरा, और सूखे मेवों को साथ बनाया जाता है।
नवाबों को मिठाइयों का बहुत शौक होता था और लखनऊ भी इसी भावना का प्रतीक है। खाने में एक लोकप्रिय व्यंजन, जो मुख्य भोजन का हिस्सा लगता है, पर होता एक मीठा व्यंजन है, वो और कोई नहीं बल्कि प्रसिद्ध शीरमल है, जोकि आटे, दूध और खमीर से बना एक मीठा नान होता है। इस मीठे नान को चाय के साथ, और कुछ कबाबों के साथ, उनके मसाले के स्तर को संतुलित करने के लिए, परोसा जाता है।
1800 के ज़माने से मिलने वाला मलाई-पान या बालाई-की-गिलौरी नामक शहर के प्रसिद्ध पान के बिना लखनवी भोजन अधूरा रहता है! देश के बाकी हिस्सों में आमतौर पर मिलने पान से अलग इस विशेष पान की सामग्री को लपेटने के लिए पान के पत्ते का नहीं बल्कि मलाई का उपयोग किया जाता है। मलाई, एक प्रकार की थक्केदार मलाई, को तब तक पीटा जाता है जब तक कि यह कागज़ जैसी पतली ना हो जाए और फिर विभिन्न सूखे मेवों, मिश्री (चीनी के कण) और गुलाब जल से भर दिया जाता है।
इन्हें भी पढ़ें –